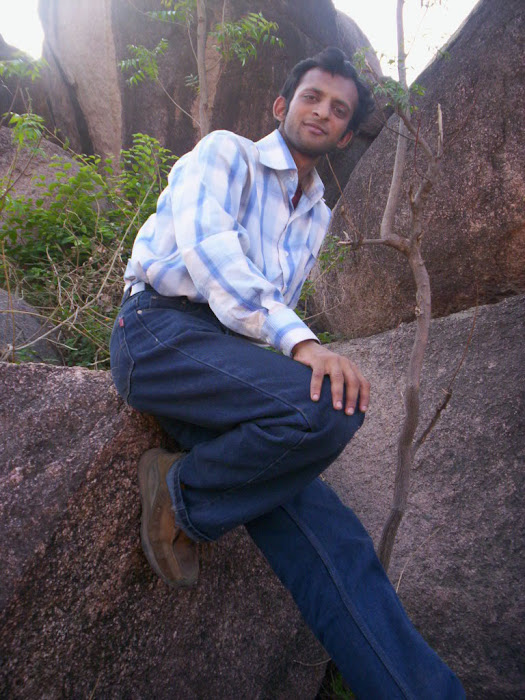धूमिल की एक कविता है, ‘जो असली कसाई है, उसकी निगाह में तुम्हारा यह तमिल दुख, मेरी भोजपुरी पीड़ा का भाई है। भाषा उस तिकड़मी दरिन्दे का कौर है, जो सड़क पर और है, संसद में और है।’
भाषा को लेकर होने वाली बहस सामाजिक भी है और राजनीतिक भी। इस बात में अब विमर्श की गुंजाइश नजर नहीं आती लेकिन भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसके महत्व को हमें स्वीकारना होगा। यूनेस्को की माने तो दुनिया भर में बोली जाने वाली 6900 भाषाओं में पचास फीसदी भाषाएं खतरे में हैं, और एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक दो सप्ताह में एक भाषा औसतन खत्म हो रही है। मात्र अस्सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, हिन्दी, मंडेरिन, रसियन जिसे विश्व भर के अस्सी प्रतिशत लोग बोल रहे हैं। दुनिया भर में 96 प्रतिशत भाषाआंे को सिर्फ चार फीसदी लोग बोल रहे हैं और 90 प्रतिशत भाषाओं का प्रतिनिधित्व इंटरनेट पर मौजूद नहीं है।
आज से लगभग अस्सी साल पहले भारत मंे एक भाषायी सर्वेक्षण सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। आज भी भाषायी सर्वेक्षण पर जब बात आती है तो लोग संदर्भ के तौर पर ग्रियर्सन को ही उद्धृत करते हैं। ग्रियर्सन के बाद देश में भाषा को लेकर उस तरह का कोई दूसरा सर्वेक्षण नजर नहीं आता।
अब पिछले ढाई-तीन सालों से बिना किसी सरकारी मदद के और बिना किसी विदेशी मदद के देश भर में भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण का काम नागरिक समाज की तरफ से हो रहा है। इसी जन भाषा सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट बताती है कि देश मंे तीन सौ से अधिक भाषाएं लापता हैं। इन्हें बोलने वाले कहां हैं, इसकी जानकारी सर्वेक्षण टीम को नहीं मिल पाई है। भाषा सर्वेक्षण का काम जारी है, आने वाले समय में हो सकता है, इस सर्वेक्षण से और भी चौकाने वाले तथ्य सामने आएं।
21-22-23 सितम्बर को दिल्ली में जनभाषा सर्वेक्षण के नेशनल कलेक्टिव में जैसे-जैसे सवाल एक के बाद एक विमर्श के लिए सामने आए, भाषा को लेकर समाज की संवेदना और लगाव की बात भी स्पष्ट होती गई। यह ‘जन भाषा सर्वेक्षण’ का अंतिम ‘नेशनल एडिटोरियल कलेक्टिव’ था। देश भर के अलग-अलग राज्यों से भाषा सर्वेक्षण के संयोजक इस आयोजन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे भाषा सर्वेक्षण की एक रूप रेखा उम्मीद है कि अगले साल अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर 21 फरवरी तक सामने आ जाएगी।
भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण की तरफ से डा. जी एन देवी ने विश्वास दिलाया, ‘21 फरवरी को हम यह घोषणा कर देंगे कि बच्चे का जन्म हो गया है। भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण की एक रूप रेखा हमारे सामने उस वक्त तक आ जाएगी।’
भारतीय जन भाषा सर्वेक्षण पिछले ढाई-तीन सालों में लगे 3500 लोगों के श्रम का नाम है, जिन्होंने 68 वर्कशॉप से 631 भाषा/बोली पर काम पूरा किया। इन भाषाओं पर अब तक लगभग 9500 पृष्ठ लिखा गया है और अभी देश भर के भाषा प्रतिनिधि अपने-अपने राज्य के सर्वेक्षण को पूरा करने में और लिखने का काम पूरा करने में लगे हुए हैं।
631 प्रविष्टियों में एक प्रविष्टि को जन भाषा सर्वेक्षण ने अब मंजूरी दी है, यह भाषा उन पचास लाख लोगों की भाषा है, जो खुद को बोलकर अभिव्यक्त नहीं करते। वे संकेत के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करते है। उनके लिए अभिव्यक्ति माध्यम संकेत है। इस भाषा का इस्तेमाल देश भर के बोल और सुन ना पाने वाले करते हैं।
तीन दिन की बातचीत में एक-एक करके कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बंगाल से आए मित्रों ने बेदिया समाज की भाषा की बात की, जिन्होंने अपनी भाषा को गुप्त भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया और आज भी बेदिया समाज के लोग अपनी भाषा के संबंध में अधिक बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनके समाज के बाहर के लोगों को इस भाषा के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है। बंगाल की बेदिया समाज की भाषा अकेली ऐसी भाषा नहीं है, इस देश में दर्जनों ऐसी भाषाएं हैं, जिनकी लिपी और साहित्य के संबंध में कोेई जानकारी नहीं मिलती। अंग्रेजों ने कई जातियों को अपराधी जाति घोषित किया था, अंग्रेजों से बचने के लिए कई अपराधी कही जाने वाली जातियों ने अपनी गुप्त बोली ईजाद की, अंग्रेज चले गए लेकिन वे बोलियां आज भी समाज के बाहर के लोगों के लिए गुप्त ही हैं।
भाषा और बोली का मामला बेहद संवेदनशील है, कोंकणी को लेकर लिपी की लड़ाई है। कुछ इसे रोमन में लिखना चाहते हैं और कुछ देवनागरी के तरफदार हैं। इसी प्रकार कई बोलियों को मिलाकर इस्तेमाल की जा रही राजस्थानी बोली को लेकर राजस्थान में कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं।
दूसरी तरफ दस हजार से कम बोली जाने वाली बोलियों का कोई रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में भी दर्ज नहीं होता। बड़ी संख्या में भाषाएं खत्म हुई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई।
ऐसे समय में जन भाषा सर्वेक्षण की यह पहल, भाषाओं और बोलियों को पहचानने और उनकी पहचान को और पुख्ता करने का ही काम कर रही है।